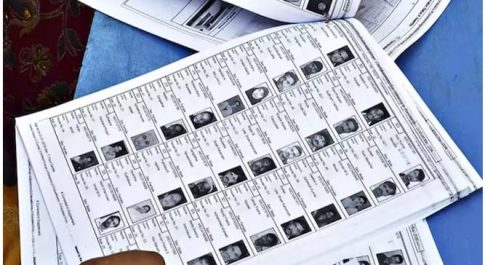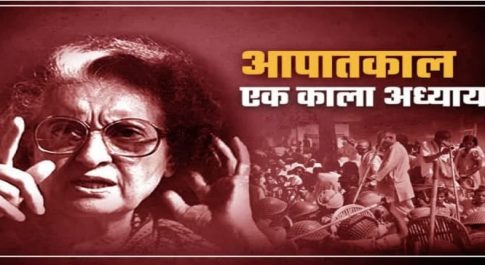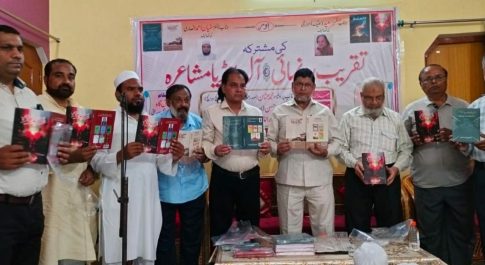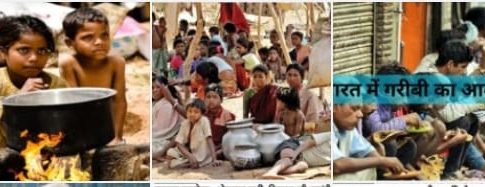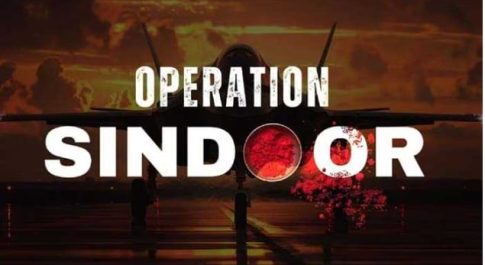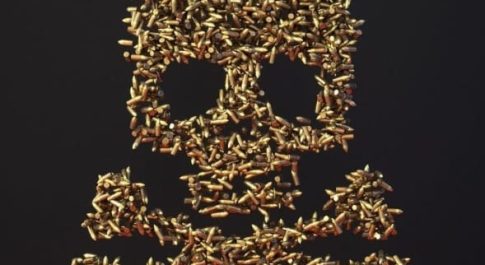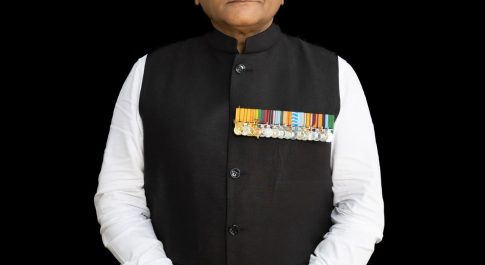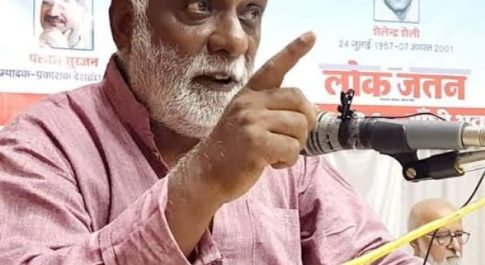कोई भी कानून अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कानून के नियम सामान्य होते हैं अतः वे उन सभी असुविधाओं के खिलाफ जिनकी संख्या अनिश्चित होती हैं, सब काल के लिये नियम नहीं बना सकते हैं क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न मामले उत्पन्न होते रहते हैं । कोई भी संहिता चाहे वह कितनी ही बुद्धिमानी से क्यों न बनाई गई हो फिर भी सभी घटनाओं के लिये और सभी समयों के लिये नियम नहीं बना सकता। साधारणतया विधान मण्डल भी सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकता। वह स्वाभाविक और सामान्य प्रसंगों का अनुमान करते हुये ही विधियों का निर्माण करता है। कोई भी मनुष्य भविष्य की घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकता, इसलिये न्यायालय के सामने ऐसे मामलों के निपटारे के लिये न्यायालय को कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जिन्हें न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ कहा जाता है। ये शक्तियाँ न्यायालय को साम्य, न्याय एवं शुद्ध अन्तकरण (Equity Justice and Good Conscience) के आधार पर वादों का अवधारण करने के लिये सशक्त करती हैं परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उन शक्तियों का प्रयोग न्यायालय तभी कर सकेगा जबकि संहिता में इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न की गई हो ।
न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों से हमारा तात्पर्य ऐसी शक्तियों से है जो न्यायालय को ऐसे मामलों के निपटारे के लिये प्रदान की जाती हैं जिनके बारे में विधि में कोई उपबन्ध नहीं दिये गये हैं । वहाँ न्यायालय साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंत: करण के आधार पर वाद तय करते हैं। न्यायालय अपनी इन अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये न तो विधि के स्पष्ट उपबन्धों को अधिभूत कर सकता है और न ही वह ऐसी कोई बात कर सकता है जो विधि द्वारा वर्जित हो । अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि संहिता के विशिष्ट उपबन्ध मामले की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यवस्था की गई है।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments