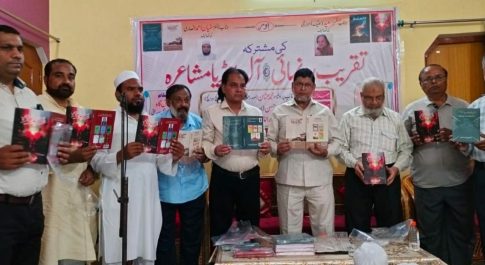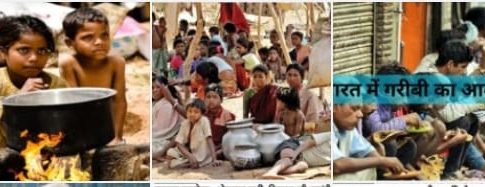रिपोर्ट : जवरीमल्ल पारख
1965 के भारत-पाक युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नॉलजी के साथ आज की स्थितियों की तुलना नहीं हो सकती, पर युद्ध से जुड़ी आशंकाएँ, अफ़वाहें, दहशत और अनिश्चितताएँ आज भी वैसी ही हैं। यह संस्मरण पहली बार 18 जुलाई, 2020 को लिखा गया था। उस समय अपने बचपन की यादें लिख रहा था और यह उसी का हिस्सा था। आज जब देश में युद्धोन्माद बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस संस्मरण को पढ़कर समझा जा सकता है कि आम आदमी के लिए भी युद्ध का क्या मतलब है।
1962 में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ, तब मेरी उम्र सिर्फ़ दस साल की थी। इतनी समझ आ चुकी थी कि चीन ने युद्ध द्वारा हमारी हज़ारों किलोमीटर ज़मीन हथिया ली है। पाकिस्तान की तरह वह भी हमारा दुश्मन देश है। उस समय देश-भक्ति के गीत और उन पर बनी फ़िल्में दिखायी जाती थीं। लोगों में देशभक्ति की भावना को उभारा जाता था और लोगों को देश के लिए अधिक से अधिक सहायता कोष में दान देने के लिए प्रेरित किया जाता था ; लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान दे भी रहे थे, जिनकी कहानियाँ अख़बारों में छपती थीं। हमारे दिमाग़ों में बैठा दिया गया था कि पाकिस्तान और चीन हमारे शत्रु देश हैं, जिन्होंने हमारे देश की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर रखा है। एक दिन हमें इनसे अपनी ज़मीन छीननी होगी। लेकिन युद्ध की कोई साफ़ तस्वीर नहीं बनी थी। बस इतना ही कि युद्ध सैनिकों के बीच लड़ा जाता है। दोनों तरफ़ से एक-दूसरे पर गोलियाँ और गोले बरसाये जाते हैं। दोनों तरफ़ के सैनिक मारे जाते हैं। हमारे सैनिक ज़्यादा बहादुर हैं। अगर हमारा एक सैनिक मरता है, तो वह चीन के दस सैनिक मार के मरता है : ‘एक-एक ने दस को मारा, फिर गये होश गँवाके’। चूँकि उनकी सेना बड़ी थी, हम हार गये। बाद में इस तरह की बातें बहुत बचकानी लगने लगीं। शायद सभी देशों के लोग दुश्मनों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं।
1965 में एक बार फिर लड़ाई हुई, लेकिन इस बार पाकिस्तान से। उस समय मेरी उम्र तेरह साल की थी और नवीं क्लास का छात्र था। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठिये भेज दिये थे, जिन्हें पीछे खदेड़ने के लिए युद्ध हुआ था। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि युद्ध सीमाओं पर ही नहीं लड़ा जाता और युद्ध के शिकार केवल सैनिक ही नहीं होते, आम नागरिक भी होते हैं। जोधपुर राजस्थान का एक सीमावर्ती शहर है। युद्ध शुरू होने के पहले दिन से ही शहर पर हवाई हमले होने शुरू हो गये थे। जोधपुर का हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। तब जोधपुर में लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग का कालेज भी था। जोधपुर के लोग लड़ाकू विमानों की चीखती आवाज़ों से और उन्हें तेज़ी से उड़ते हुए और तरह-तरह के करतब करते हुए देखने के आदी थे।
जब पाकिस्तान के बमवर्षक विमान बी-57 शहर की तरफ़ बढ़ते थे, तो उसके कुछ सैकंड पहले सायरन बजती थी। यह इस बात का संकेत होता था कि लोग अपने घरों की बत्तियाँ बंद कर लें। खाइयों में दुबककर बैठ जायें और तब तक बैठे रहें जब तक कि सायरन दुबारा न बजे, जो इस बात का संकेत होता था कि दुश्मन के विमान लौट गये हैं। विमानों के आने के समय बजने वाला सायरन रुक-रुक कर बजता था, जैसे बार-बार चेतावनी दी जा रही हो। ख़तरा टलने का सायरन ऐसे बजता था, जैसे रास्ता साफ़ हो गया हो। जोधपुर में शक्तिशाली राडार प्रणाली लगी हुई थी, जो पाकिस्तानी विमानों की पहचान जल्दी कर लेता था।
हमारे घर से हवाई अड्डा तीन-चार किलोमीटर ही दूर था और हवाई हमले का मुख्य लक्ष्य वह हवाई अड्डा ही था। घर शहर के मध्य एक गली में था, जहाँ न खाइयाँ खोदी जा सकती थीं और न ही घरों में बेसमेंट बने हुए थे। गली में हमारे घर से चार मकान दूर एक हवेलीनुमा बड़ा-सा मकान था जिसे मारवाड़ी में नोहरा कहा जाता है। नोहरे के बड़े-से फाटक के अंदर बने मकान के आगे की तरफ़ खुला मैदान-सा था। मैदान आकार में बहुत छोटा ही था। लेकिन वहाँ दो-तीन खाइयाँ खोदी गयी थीं। गली में मुसलमानों के लगभग 70-80 घर थे और हिंदुओं के दस-बारह। इस खुली जगह और खाइयों का उपयोग हिंदू ही कर रहे थे। वहाँ मैंने कभी किसी मुस्लिम परिवार को नहीं देखा था। शायद उन्हें वहाँ आने के लिए कहा ही नहीं गया या वे अपनी इच्छा से नहीं आ रहे थे। गली में एक-दो छोटे नोहरे मुसलमानों के भी थे। शायद वहाँ भी खाइयाँ खोदी गयी हों। लेकिन न हिंदुओं के लिए और न ही मुसलमानों के लिए वे खाइयाँ पर्याप्त थीं। केवल बूढ़े और बच्चों के लिए ही इनका इस्तेमाल हो सकता था। बच्चों के लिए उनमें सिर नीचा करके बैठना खेल की तरह होता था। वे थोड़ी-थोड़ी देर बाद खाई से बाहर निकाल कर देखने लगते थे। तभी किसी बड़े की डाँट पड़ती और फिर से वे सिर नीचा कर लेते थे। हमारे घर से मेरे दादा और बच्चों को भेजा जाता था। एक-दो बड़े भी साथ भेजे जाते थे। लेकिन पूरी रात वहीं बैठे रहना अजीब लगता था। इसलिए सायरन होने पर भाग कर जाते थे और ख़तरा टलने पर वापस लौट आते थे। यह क़वायद मुझे अजीब लगती थी और मैंने एक-दो दिन बाद ही जाना बंद कर दिया।
हमारा घर भी अपेक्षाकृत बड़ा था, लेकिन उसमें खाई नहीं खोदी जा सकती थी। इतना ही कर सकते थे कि घर की निचली मंज़िल पर दीवार के सहारे कोनों में दुबक कर बैठ जायें। कानों में रुई ठूँस लें, ताकि बम गिरने की तेज़ आवाज़ के कारण कान के पर्दे न फट जायें। इन सब बातों का प्रचार सड़कों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से होता था, जिनसे सायरन की आवाज़ भी आती थी। सरकार की तरफ़ से पूरे शहर में जीपें भी घूमती थीं, जो लाउडस्पीकर पर लोगों को ब्लेक आउट रखने, खाइयों में बैठने या घरों में ही सुरक्षित जगह पर बैठने की हिदायत देते थे। कई युवा इन कामों के लिए स्वेच्छा से आगे आये थे और वे पूरी रात गलियों और सड़कों पर घूमकर निगरानी रखते थे। जब हम नोहरे में नहीं जाते थे, तब हम बच्चों को कोने में दुबका दिया जाता था और कुछ चारपाइयों के नीचे लेट जाते थे। डर भगाने के लिए हमें कहा जाता था कि मन में हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब ख़तरा टल जाता था, तब घर के बड़े धीमी आवाज़ में भजन गाने लगते थे। डर के मारे बत्ती तब भी नहीं जलायी जाती थी। अगर किसी वजह से कोई जलाता तो सब एक साथ चीख़ पड़ते। अंधेरे के साथ चारों ओर डर पसरा हुआ था। हम बच्चे भी डरे हुए थे, हालाँकि यह नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। क्या सचमुच बम गिरेगाॽ क्या हम सब मर जायेंगेॽ ठीक-ठीक तो यह भी नहीं पता था कि मरना क्या होता हैॽ
लड़ाकू विमानों की उड़ने की आवाज़ें आती थीं और कभी विमान बिना शोर-शराबा किये शहर की सीमा में घुस आते थे और फिर शहर के ऊपर तेज़ आवाज़ करते थे। कभी दूर, तो कभी-कभी बहुत दूर बम गिरने की आवाज़ भी आती थी। बम गिरने की आवाज़ से बस यही संतोष होता था कि हमारे आस-पास बम नहीं गिरा है। शायद कहीं आसपास के गाँव में गिरा हो, शायद कोई मरा भी हो, लेकिन तब तक धुकधुकी बँधी रहती थी, जब तक विमान वापस नहीं लौट जाते थे और ख़तरा टलने का सायरन नहीं बज जाता था। कभी-कभी सायरन बजता भी नहीं था कि विमानों के आने की डरावनी आवाज़ सुनायी देती थी और फिर कहीं ज़ोर के धमाके की। ज़्यादातर कई विमान एक साथ आते थे। और इतने नीचे से गुज़रते थे कि लगता था कि बम यहीं गिराने वाले हैं। शायद राडार से बचने के लिए ऐसा करते थे। कभी ऊँचाई से गुज़र जाते थे। हर रात दो-तीन बार इस तरह के हमले होते थे और हम सब डरे-डरे राम-राम करते रात गुज़ारते थे।
हमें यह नहीं पता लगता था कि दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए हमारी तरफ़ से क्या हो रहा है। वे विमान सब कहाँ चले गये, जो शांति के दिनों में आकाश में उड़ते नज़र आते थे या अब भी दिन में उड़ाने भरते थे। शायद शहर के लोगों को आश्वस्त करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं हम हैं। लेकिन रात को दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए कोई नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था, जैसे उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लगता था शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। युद्ध के बाद मालूम हुआ कि प्रशिक्षण देने वाले सारे विमान दक्षिण में सुरक्षित जगह पर भेज दिये गये थे।
हवाई हमले दिन में नहीं होते थे। दिन भर तरह-तरह की ख़बरों का बाज़ार गर्म रहता था। यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि रात को कहाँ बम गिरा है और कितना नुकसान हुआ है। ख़बरों में बताया जाता था कि पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन जोधपुर पर बमबारी की ख़बर कम होती थी और होती भी, तो महत्त्वहीन ढंग से। शायद भारतीय पक्ष की युद्ध योजना में जोधपुर की हवाई हमले से रक्षा शामिल नहीं थी। कम से कम लोगों का यही सोचना था। ख़बरों में यह भी बताया जाता था कि पाकिस्तान ने बम गिराये, लेकिन वह खेतों में गिरे या फटे नहीं और कोई नुक़सान नहीं हुआ। लोगों के बीच इस बात का मज़ाक़ भी बनता था कि पाकिस्तान के विमान चालकों को निशाना लगाना नहीं आता था। लोगों का यह भी मानना था कि शहर की चामुंडा देवी, जिनका किले में मंदिर था, वे चील बनकर शहर की रक्षा कर रही हैं। यह मान्यता इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि लगता था, पूरा शहर इसमें यक़ीन करता है। यह और बात है कि युद्ध के अंतिम दिन गिरे बम से जेल अस्पताल के मरीज मारे गये थे। लोगों का मानना था कि वे पापी थे, इसलिए माँ ने उनकी रक्षा नहीं की। लेकिन 43 साल बाद 30 सितंबर 2008 को उसी देवी के मंदिर का दर्शन करने के लिए जमा हुई देवी के भक्तों की भीड़ में भगदड़ मच गयी थी और 224 लोग मारे गये थे और 425 से ज़्यादा लोग घायल हो गये थे। वे अपराधी थे या नहीं, लेकिन देवी के भक्त ज़रूर थे।
युद्ध के उन दिनों में बहुत तरह की अफ़वाहें उड़ती थीं। ज़्यादातर मुसलमानों के बारे में होती थी कि फ़लाने मुस्लिम मोहल्ले में टार्च की रोशनी फैंक कर इशारा किया जाता है। आमतौर पर हिंदू मानते थे कि मुसलमानों की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है। यह भी अफ़वाह फैलायी गयी कि उपराष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन का कोई रिश्तेदार जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। हमारे मोहल्ले के आसपास एक पागल-सा आदमी घूमा करता था, उसके बारे में भी सुना गया कि उसे भी पकड़ लिया गया है, क्योंकि वह पाकिस्तान का जासूस है। हालाँकि युद्ध के बाद उस पागल को पहले की तरह टहलते देखा था। इन अफ़वाहों के स्रोत क्या थे, यह उस समय नहीं मालूम था। और यह जानने का भी कोई तरीक़ा नहीं था कि इनमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। भारतीय जनसंघ के नाम से तो परिचित था, लेकिन आरएसएस के नाम से नहीं। बहुत सालों बाद यह समझ आया कि इन अफ़वाहों का एक ही स्रोत था, जिसका मक़सद हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करना होता था। वे आज भी यही काम करते हैं। बस, फ़र्क़ यह है कि आज वे सत्ता पर काबिज भी हैं और इस नफ़रत की आग ने ही उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुँचाया है। युद्ध के उस दौर में लोग आकाशवाणी से समाचार सुनते थे, लेकिन उन पर यक़ीन नहीं करते थे। सही समाचारों के लिए बीबीसी सुना करते थे।
जिस गली में हमारा मकान था, उस गली में ज़्यादातर मकान मुसलमानों के थे। लेकिन मैंने देखा कि उनके घरों में भी घुप अंधेरा रहता था। डर उनके यहाँ वैसा ही पसरा हुआ था, जैसा हमारे यहाँ। मेरे दिमाग़ में यह भी आता था कि अगर हमारी गली में बम गिरा तो हम सब मरेंगे, हिंदू भी और मुसलमान भी। जब मुसलमानों के बारे में बात की जाती थी, तो हमें लगता था कि किसी और मोहल्ले के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। रात को जब ख़तरा टलने का सायरन बजता था, तो कुछ लोग घरों से बाहर आकर आपस में बातचीत करते थे। सबकी एक ही शिकायत थी कि पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने के लिए हमारे विमान क्यों नहीं जाते। कुछ लोग सायरन के दौरान भी अपने घरों की छतों पर बैठे रहते थे और किले के पीछे से पाकिस्तानी विमानों को आते और जाते देखते थे और फिर दिन में बताते थे कि कुल कितनी बार कितने विमान आये। विमानों की तेज़ आवाज़ दिल की धड़कनें बढ़ा देती थीं। मन ही मन बोली जाने वाली हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ होठों से बाहर निकल आती थीं। फिर किसी बड़े की फुसफुसाती डाँट से वापस मुँह में चली जाती थीं।
कुछ दिनों बाद शहर के आसपास विमान भेदी तोपें तैनात कर दी गयी थीं। जैसे ही सायरन बजता, तोपों से गोले छूटने लगते थे, जिससे पूरा आकाश आच्छादित हो जाता था। तोपों से थोड़ा सुकून मिला था कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन कभी यह समाचार सुनने को नहीं मिला कि उन गोलों से कोई विमान गिरा हो। हवाई हमले पहले की तरह जारी थे। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना हुआ कि रात के सन्नाटे को तोड़ती सायरन की आवाज़, विमानों की हल्की गूँजती आवाज़ और उन डरावनी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करतीं तोपों की आवाज़ें कुछ आश्वस्त करती लगती थीं। लेकिन तभी उन सब आवाज़ों को दहलाता हुआ बम का धमाका होता था और इसके साथ ही डर स्थायी भाव की तरह फिर आ जमता था।
युद्ध तेज़ होता जा रहा था। हवाई हमले भी बढ़ते जा रहे थे। अभी तक शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सैनिक ठिकानों को कोई नुकसान हुआ हो तो पता नहीं लगता था। लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। मेरे दादा सबसे ज़्यादा डरे हुए थे और पूरी रात उनकी हाय-हाय करते गुज़रती थी। दादी काफ़ी हिम्मत वाली थीं, लेकिन उनकी चिंता यह थी कि बम गिरा और घर नष्ट हो गया, तो घर में पड़े गहने-जेवरात लोग लूट ले जायेंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने पहनने वाले वस्त्रों में जेबे बना ली थीं और गहने उसमें छुपा दिये थे, ताकि भागना भी पड़े तो जेवरात बचे रहें। हम बच्चे तो सिर्फ़ डरे हुए ही थे, लेकिन बड़े-बूढ़े तनाव में से भी गुज़र रहे थे। यह तनाव उनके व्यवहार में अजीब-अजीब ढंग से दिखायी देता था। कुछ पहले से ज्यादा चिड़चिड़े हो गये थे। कुछ बच्चों को इस डर से निकालने की बजाय खुद इतने डरे हुए थे कि अपने डर को बच्चों को डाँटने-पीटने के द्वारा निकालते थे। हम कुछ बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे, दिन में स्कूल जाते थे। लेकिन कक्षा में जो पढ़ाया जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। या तो रात की बातें याद आती थीं या रात भर जगने के कारण कक्षा में ही झपकियां आने लगती थीं और अध्यापकों से डाँट खानी पड़ती थीं। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि अघ्यापकों का मन भी पढ़ाने में नहीं लग रहा था।
डर के मारे कुछ लोग शहर छोड़कर दूसरे शहरों-गाँवों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे थे। खासतौर पर घर के बूढ़े, बच्चों और औरतों को भेजा जा रहा था। मेरी बुआ का परिवार, जो जयपुर के पास एक कस्बे नावा शहर में रहता था, वहाँ भेजे जाने का विकल्प मौजूद था। बुआ ने सभी को यहीं आ जाने का संदेश भिजवाया था। मेरे दादा तो इस डर के कारागार से किसी भी क़ीमत पर निकलना चाहते थे। जिन्होंने कभी बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पिया था, वे वहाँ जाकर रहने के लिए तैयार थे। दादी किसी भी क़ीमत पर अपना घर छोड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाये। दादा दबाव डाल रहे थे कि जब बम गिरेंगे और मर जायेंगे, तो क्या होगा। दादी का कहना था कि ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बम क्या सिर्फ़ हमारे घर पर ही गिरेगा। घर में चूँकि दादी की ही चलती थी, दादा चिड़-चिड़ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी शिकायत यह भी थी कि चारों बेटे अपनी माँ की ही मानते हैं, बाप को तो कुछ समझते ही नहीं।
लेकिन आख़िर एक दिन जाने का फ़ैसला हो गया। हवाई हमले के सात-आठ दिन बाद संभवत:14 सितंबर की रात थी, उस दिन एक ही रात में चालीस बम गिरे। पूरी रात बम के धमाकों की आवाज़ आती रही। कुछ बम तो इतने पास गिरे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ दुगुनी गति से होने लगा था। लग रहा था कि अगला बम तो हमारे घर पर ही गिरने वाला है। किसी तरह रात गुजरी। बम बरसा के पाकिस्तानी विमान लौट चुके थे। तरह-तरह की ख़बरें आने लगीं। मालूम पड़ा कि हमारी गली से मुश्किल से एक किलोमीटर दूर स्टेशन और कालटेक्स पेट्रोल पंप के पास भी दो-तीन बम गिरे थे, लेकिन वह फटे नहीं थे। इस सूचना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। उस दिन शहर छोड़कर जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गयी। अब हमारी दादी ने ही फ़ैसला कर लिया कि सभी बच्चों, तीनों बहुओं और दादाजी को बुआ के यहाँ भेज दिया जाए। दादी ने कहा कि वह यहीं रहेंगी। बड़े चाचा इसलिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी करते थे। प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी एक व्यक्ति का रुकना ज़रूरी था, इसलिए पिताजी भी ने भी घर पर रहने का फ़ैसला किया। लेकिन साथ में किसी बड़े, समझदार और हिम्मत वाले व्यक्ति का जाना भी ज़रूरी था। इसलिए दूसरे नंबर के चाचा के संरक्षण में उसी दिन सबको रवाना कर दिया गया। हम बच्चे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बमबारी में जितना डर था, उतना रोमांच भी था और स्कूल से गैर हाजिर होने पर पढ़ाई का नुकसान होने का डर भी था। कहीं यह भी मन में था कि लोग हमें भगोड़ा समझेंगे। हमने नहीं जाने के लिए चूं-चा भी की, लेकिन इस मामले में हमारी राय का कोई मतलब नहीं था। वे बहुएँ (जैसे मेरी माँ) भी नहीं जाना चाहती थीं, जिनके पति यहीं रहने वाले थे। लेकिन उनको बच्चों का हवाला देकर राज़ी कर लिया गया। इस तरह 17 लोगों के भरे-पूरे परिवार में से तीन को छोड़कर सबको भेज दिया गया।
हम युद्ध के मैदान में से तो निकल आये थे, लेकिन डर और तनाव ने पीछा नहीं छोड़ा। पहुँचने के दूसरे दिन से ही उन सबकी चिंता सताने लगी जिन्हें पीछे छोड़ आये थे। संचार के साधन इतने नहीं थे कि हर दिन हर पल की ख़बर मिले। युद्ध अब भी जारी था और जोधपुर पर बमबारी भी। शुरू में धीमे-धीमे बाद में वापस लौटने की आवाज़ें तेज़ होने लगी। हमें अपनी स्कूल और पढ़ाई की चिंता सताने लगी। बुआ ने कहा कि जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक सब शांति से रहो। दादा जी भी वापस लौटने की रट लगाने लगे, क्योंकि उन्हें अब दादी की चिंता सताने लगी थी। इस तरह सात-आठ दिन गुजर गये। और एक दिन फिर भीषण बमबारी हुई। जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास ही बनी केंद्रीय जेल के अस्पताल पर बम गिरा और कई मरीज़ इस हमले में मारे गये। शायद तीस-बत्तीस लोग। इसने फिर दहशत बढ़ा दी और सब ज़िद करने लगे कि हमें तो जोधपुर जाना है। और युद्ध ख़त्म होने से पहले ही लौटने का फ़ैसला कर लिया गया। युद्ध विराम की चर्चा भी थी और जोधपुर पहुँचते-पहुँचते युद्ध विराम लागू भी हो गया। जब स्टेशन से तांगे में घर की ओर लौट रहे थे, तो लोगों ने फब्तियाँ भी कसीं। जब हम बुआ के यहाँ गये थे, तब भी शहर से काफ़ी लोग पलायन कर चुके थे। पिताजी का कहना था कि लगभग आधा शहर ख़ाली हो गया था।
उस समय समाचारों के अनुसार युद्ध की पूरी अवधि में जोधपुर और उसके आसपास दो लाख पौंड के ढाई सौ से ज़्यादा बम गिराये गये थे। हवाई अड्डे या हवाई पट्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जेल अस्पताल पर गिरे बम ने ज़रूर कई बीमार लोगों की जान ले ली। युद्ध का जो भी नतीजा निकला हो, लेकिन वह पंद्रह-बीस दिन दहशत भरे थे। हम आम आदमी तो इन हवाई हमलों के शिकार ही हो सकते थे, जैसे जेल के मरीज़। न हम मुक़ाबला कर सकते थे और न ही अपनी रक्षा। मैदान छोड़कर भाग सकते थे, जैसे हम भागे थे।
दिन बीतते गये, हवाई हमलों की रातें स्मृतियों में रह गयी थीं। सब कुछ सामान्य होता चला गया था। इसके छह साल बाद एकबार फिर पाकिस्तान का हवाई हमला जोधपुर पर हुआ। अभी साँझ का झुरमुटा ही फैला हुआ था कि एक बार फिर किले की तरफ से पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज जोधपुर आ पहुँचे। इन छह सालों में जोधपुर के आसपास एक छावनी-सी विकसित हो गयी थी। उन विमानों को मालूम था कि उन्हें कहाँ हमला करना है और बनाड़ के पास छावनी वाली जगह पर जहाँ तेल के भंडार भी थे, बमबारी करके जितनी तेज़ी से आये थे, उतनी ही तेज़ी से चले भी गये। सायरन ज़रूर बजा। लेकिन लोगों को संभलने का मौक़ा नहीं मिला। तेल की लपटें आकाश को छूने लगीं। लोग छतों पर खड़े होकर देख्नने लगे। लोगों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या एक बार फिर से 1965 वाले हालात से गुज़रना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह हवाई हमले की पहली और आख़री रात थी। फिर कोई पाकिस्तानी जहाज जोधपुर तक नहीं पहुँच पाया और लोग युद्ध की चर्चा मज़े ले-लेकर करने लगे। बातों से ही लोग पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में लगे थे।
कभी-कभी सोचता हूँ, आज दोनों देश आणविक हथियारों से लैस हैं और 1965 और 1971 की तुलना में एक दूसरे पर हमला करने के कहीं ज़्यादा साधन उनके पास हैं और इन हथियारों से वे एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। बस ज़रूरत ऐसे युद्धोन्मादी बुद्धिहीन शासकों की हैं, और शायद ऐसे शासकों से आज हम बहुत दूर भी नहीं हैं। तब हमारा यह सीमावर्ती शहर जोधपुर एक आसान निशाना बन सकता है।
*(‘नया पथ’ से साभार। लेखक जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। संपर्क : [email protected], (मो) : 98106-06751)*
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments