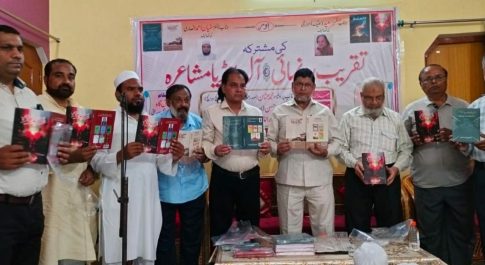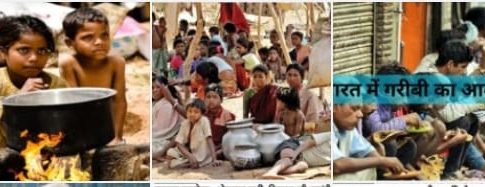रिपोर्ट : प्रभात पटनायक
अनुवाद : लाल बहादुर सिंह
कोई यह दावा नहीं कर सकता कि नवउदारवादी दौर में, उससे पहले के लोककल्याणकारी राज्य के दौर की तुलना में, कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि हुई है। यह सच है कि पहले की तुलना में जीडीपी में तेज वृद्धि हुई है, भले ही दावे उतने सटीक न हों। लेकिन लोककल्याणकारी दौर में खाद्यान्न की कीमतों पर लगातार दबाव रहता था, जो इस बात का संकेत था कि खाद्यान्न की मांग अधिक थी। इस मांग को मूल्य नियंत्रण या कई अवसरों पर सरकारी खर्च में कटौती के जरिए संभाला जाता था।
नवउदारवादी दौर में सरकार के पास खाद्यान्न भंडार का अंबार रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित अनाज से कहीं अधिक संग्रह होता था। इतना कि सरकार खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगी—2023-24 में चावल का निर्यात 10.4 अरब डॉलर का था।
इस विरोधाभास की व्याख्या कैसे होगी कि देश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बढ़ रही थी, जबकि खाद्यान्न उपभोग की वृद्धि दर घट रही थी? नवउदारवादी प्रवक्ताओं को इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। उनका तर्क है कि जैसे-जैसे लोग समृद्ध होते हैं, उनकी आय वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न उपभोग में वृद्धि कम होती है। इसलिए, उनके अनुसार, खाद्यान्न बाजार में सरप्लस का कारण यह है कि नवउदारवाद के तहत सभी की स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन यह तर्क तथ्यों के विपरीत है।
आय बढ़ने पर लोग प्रत्यक्ष खाद्यान्न उपभोग कम कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (प्रोसेस्ड फूड और पशु चारे के रूप में) खाद्यान्न का कुल उपभोग कम नहीं हो सकता। बल्कि, यह बढ़ना चाहिए। फिर भी, तथ्य बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग घटा है। न्यूनतम आवश्यक कैलोरी न मिलने वालों की संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में 1993-94 में 58% लोग प्रतिदिन 2200 कैलोरी से कम उपभोग करते थे, जो 2017-18 में बढ़कर 80% हो गया।
इसलिए, नवउदारवादी दौर का खाद्यान्न सरप्लस समृद्धि का नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग की बढ़ती दरिद्रता का प्रतीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और महिलाओं में रक्ताल्पता के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं।
हमारे सामने विकास के दो प्रतिमान हैं। पहला, लोककल्याणकारी मॉडल, जिसमें खाद्यान्न की कमी रहती थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि कुल वृद्धि दर खाद्यान्न वृद्धि दर से अधिक नहीं हो पाती थी। बढ़ी आय के कारण खाद्यान्न मुद्रास्फीति बढ़ जाती थी।
दूसरा, नवउदारवादी मॉडल, जिसमें खाद्यान्न का अतिरेक है। यहां कुल वृद्धि दर को निर्यात बाधित करता है। कोई देश तभी तेजी से विकास कर सकता है, जब विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, और वह देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे या अन्य देशों की कीमत पर इसे बढ़ाए। विश्व बाजार की तीखी प्रतिस्पर्धा के कारण तेज विकास में तकनीकी और ढांचागत बदलाव अंतर्निहित होते हैं, जो श्रम की बढ़ी उत्पादकता में प्रकट होते हैं। इसका परिणाम रोजगार में मामूली वृद्धि होता है, जो नए बेरोजगारों, सरकारी संरक्षण खत्म होने से पुराने बेरोजगारों, और विस्थापित किसानों व कारीगरों की संख्या से हमेशा कम रहता है।
श्रम बल की तुलना में आरक्षित श्रम बल बढ़ता जाता है, जिससे मजदूरों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटती है। यह आय कमी ही खाद्यान्न सरप्लस का मूल कारण है।
*निष्कर्ष और वैकल्पिक मॉडल*
*नया पैमाना* : प्रति व्यक्ति जीडीपी को प्रगति का पैमाना मानने के बजाय, लोगों के कल्याण को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं (विशेष रूप से खाद्यान्न) का उपभोग पैमाना बनाना चाहिए। लोककल्याणकारी दौर में यह उपभोग घरेलू उत्पादन के समतुल्य था, जबकि नवउदारवादी दौर में क्रय शक्ति घटने से मांग सीमित हो गई।
*रोजगार वृद्धि* : खाद्यान्न सरप्लस का उपयोग रोजगार बढ़ाकर और आवश्यक वस्तुओं की खपत बढ़ाकर किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी खर्च बढ़ाना होगा, जो दो तरीकों से संभव है: वित्तीय घाटा बढ़ाकर या धनी वर्ग पर कर बढ़ाकर। मेहनतकशों पर कर बढ़ाने से मांग का स्थानांतरण होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा।
वैश्विक पूंजी इन दोनों उपायों का विरोध करती है, क्योंकि यह उसके वर्चस्व को चुनौती देता है। इसलिए, खाद्यान्न सरप्लस और बेरोजगारी के इस विवेकहीन संकट को हल करने के लिए पूंजी नियंत्रण लागू करना होगा। यह नवउदारवादी नीतियों का अंत होगा, क्योंकि इनका आधार ही पूंजी, विशेष रूप से वित्तीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह है।
प्रति व्यक्ति जीडीपी के बजाय आवश्यक वस्तुओं के उपभोग के पैमाने से देखें, तो नवउदारवादी दौर लोककल्याणकारी दौर से बदतर है। यह रोजगार वृद्धि में बाधक, अतार्किक और विवेकहीन है।
*वैकल्पिक दृष्टिकोण*
यह कहना ठीक नहीं कि हमें पूरी तरह लोककल्याणकारी दौर में लौट जाना चाहिए। उस दौर में विकास दर खाद्यान्न उत्पादन पर निर्भर थी। रोजगार बढ़ाने के लिए खाद्यान्न की उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और सरकारी निवेश आवश्यक हैं।
भूमि सुधार को केवल सामंती संकेंद्रण तोड़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आजादी से पहले दीर्घकालीन पट्टों पर दी गई और अनुत्पादक पड़ी जमीन, जैसे प्लांटेशन, को भी भूमि सुधार के दायरे में लाना होगा।
नवउदारवादी निर्यातोन्मुखी विकास का विकल्प केवल राज्य प्रायोजित विकास नहीं, बल्कि सरकारी संरक्षण में कृषि-आधारित विकास है।
साभार : पीपुल्स डेमोक्रेसी। लेखक अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments