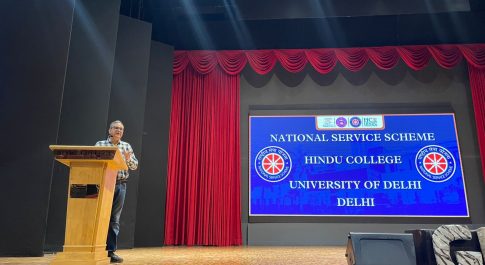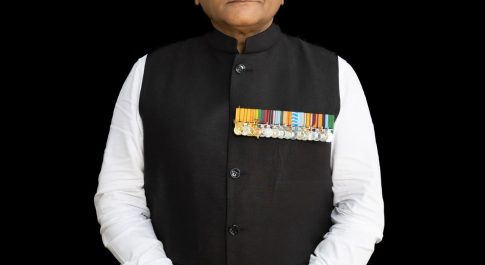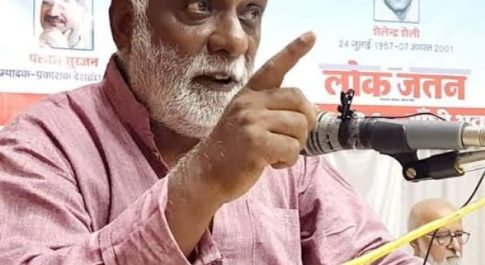रिपोर्ट : फली एस नरीमन, अनुवाद : संजय पराते
राजनैतिक दृष्टि से यह अच्छी बात है कि भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान (अनुच्छेद 370) अब प्रभावी नहीं रह गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के तीन निर्णयों (एक मुख्य और दो सहमति वाले) में 11 दिसंबर को केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है : इससे जम्मू और कश्मीर का भारत संघ में पूर्ण एकीकरण करने की सुविधा मिल गई है। अगर इतना ही हुआ होता, तो इस सर्वसम्मत फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन केवल इतना ही नहीं हुआ।h
मेरे विचार में, केंद्र द्वारा वास्तव में जो किया गया, वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं था, न ही संघवाद के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जो कि हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और जिसे 1994 में नौ न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ के फैसले में रेखांकित किया गया था।
भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 370 को 1954 के राष्ट्रपति के आदेश संख्या 48 के साथ पढ़ा जाए, तो पता चलता है कि इसके तहत एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पेश की गई थी। अनुच्छेद 3 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य पर इस शर्त के साथ लागू किया गया था कि इसका क्षेत्रफल (जो वर्ष 1950 में 39,145 वर्ग मील था — तीन निर्णयों में से किसी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है) जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा की सहमति के बगैर, न तो कार्यपालिका द्वारा कम किया जाएगा और न ही संसद के द्वारा। हालाँकि, इस आश्वासन के विपरीत, अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा राज्य विधानसभा की सहमति के बिना और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को भी जानकारी दिए बिना जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्रफल में (22836 वर्ग मील — फिर से तीन निर्णयों में से किसी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है) बहुत बड़ी कमी की गई। इससे कुछ महीने पहले, 19 दिसंबर, 2018 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र द्वारा राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन (व्यंजना के रूप में राज्य में केंद्र सरकार का शासन) लागू कर दिया गया था और इससे निर्वाचित विधान सभा में उनके प्रतिनिधियों की सहमति का सवाल टाल दिया गया था।
तीनों निर्णयों में से किसी में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल काफी हद तक कम हो गया है (जनवरी 1950 में 35,145 वर्ग मील से अगस्त 2019 में सिर्फ 16,304 वर्ग मील हो गया), इसकी स्थिति भी एकतरफा तौर पर (बहुत कम क्षेत्रफल के साथ) एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है, जो न तो जरूरी थी और न ही संविधान के किसी भी प्रावधान द्वारा उचित ठहराई जा सकती है।
जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा अनुच्छेद 370 (3) में ही निर्धारित की गई थी, जैसा कि 1950 में अधिनियमित किया गया था। यह इस प्रकार है : “(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो वह निर्दिष्ट कर सकते है : बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।”
इसलिए, अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति (जो वास्तव में, केंद्र की शक्ति है) पूरे अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित करने के लिए, केवल तभी प्रभावी होनी थी, जब अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान में पूर्व शर्त — जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफ़ारिश — पूरी हो गई हो। इसे नज़रअंदाज करते हुए और इस खंड में उल्लेखित एक प्रावधान के वास्तविक कार्य की भी उपेक्षा करते हुए, अदालत ने मुख्य फैसले में इस प्रकार कहा है : “चूंकि जब भारत का संविधान अपनाया गया था, तब तक जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, अनुच्छेद 370 (3) में उल्लेखित प्रावधान में केवल राज्यों के मंत्रालय द्वारा तय की गई अनुसमर्थन प्रक्रिया ही समाहित है। खंड (2) में संदर्भित शब्द ‘राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी’ को, अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधानों को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान सभा की सिफारिशें शुरू से ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थीं।
न्यायालय का यह निष्कर्ष कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, अनुच्छेद 370 (3) के दो अलग-अलग हिस्सों में होने की न्यायालय की गलत व्याख्या पर आधारित है। यह मुख्य निर्णय अपने निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कहता है कि अनुच्छेद 370 (3) दो अलग-अलग हिस्सों में है : “जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन पर अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। जब संविधान सभा को भंग कर दिया गया, तो अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान में केवल संक्रमणकालीन शक्ति को मान्यता दी गई। जो संविधान सभा को अपनी सिफारिशें करने का अधिकार देती थी, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इससे अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा धारित शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।”
मुख्य निर्णय में जो कहा गया है, वह न केवल अनुच्छेद 370 (3) के सीधे विपरीत है, बल्कि एआईआर 1961 एससी 1596 में रिपोर्ट किए गए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पूर्व निर्णय के विपरीत भी है। इसमें कहा गया है: “एक प्रावधान जोड़ा जाता है गुणवत्ता को अधिनियमित करने के लिए या उसके लिए कोई अपवाद बनाने के लिए या अधिनियम में क्या कुछ है, इसे बताने के लिए। सामान्य तौर पर, किसी प्रावधान की व्याख्या सामान्य नियमों के रूप में बताए जाने के लिए नहीं की जाती है।”
इसलिए, मेरा निष्कर्ष यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय भले ही राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हो, लेकिन संवैधानिक रूप से सही नहीं है।
लेखक संवैधानिक न्यायविद् और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments